क्या जीवन में कोई लक्ष्य होना आवश्यक है ?
अगर नहीं,
तो क्या हम लक्ष्यहीन जीवन को निरर्थक नहीं समझते हैं?
और अगर हां,
की, जीवन में लक्ष्य ही सब कुछ है।
तो क्या होता है लक्ष्यप्राप्ति के उपरांत?
क्यों होता है?
मनुष्य जीवन में जब एक लक्ष्य साधक बनता है।
तो वह खुद में अपने आप में संशोधन करता है।
स्वयं को अनुकूल बनाने का सतत प्रयास करता है।
एक समय बाद संभवतः
उसके लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है।
साधक जो पूर्णता की खोज में था,
क्या उसे अब वह हासिल कर पाया ?
क्या वह संतुष्टता शालीनता और शांति का प्रतिबिंब हो चुका है?
क्या वह अब सांत्वना का स्वामी है ?
क्या उसकी दृष्टिकोण अब कभी आश्रित नहीं होंगी ?
अगर नहीं,
तो क्या था उस लक्ष्य का गंतव्य ?
क्या वह कमजोर था ?
या फिर सत्य यह है कि,
उस लक्ष्य में कोई प्राण ही नहीं था?
एक अल्पविराम के पश्चात,
एक बार फिर, वह अपनी कृति दोहराता है।
एक बार फिर, वह अपने समक्ष एक नई मछली की आंख रखता है।
एक बार फिर, वह संशोधन की दिशा में आगे बढ़ता है।
एक बार फिर, साधक साधना में विलीन हो जाता है।
एक लक्ष्य प्राप्त करने से दूसरे लक्ष्य को साधने तक,
इनके बीच का अंतराल क्या है?
अगर इस क्षितिज पर हम चिंतन करें,
तो कदाचित जीवन का अर्ध सत्य हमें अल्प रूप से ही सही, पर निहारता है।
अगर,
अगर लक्ष्य वास्तविक है, तो उसका प्रतिफल इतना आंशिक क्यों ?
और,
यदि आप की प्रतीति में, वह आंशिक नहीं बल्कि पूर्ण है
तो महत्वाकांक्षाओं के बीज फिर क्यों बोए गए?
वह पूर्णता ही क्या जिसमें पूर्णता की लालसा हो।
और ,
अगर इसी अर्धसत्य का और अध्ययन करें तो मुमकिन है कि पूर्ण सत्य के निकट को हम।
लक्ष्य एक मिथ्या का पाश है।
जिसे भेदने का समर्थक केवल चेतना में है।
क्या जीवन एक परिणाम है, शायद नहीं।
क्या जीवन एक स्थान है, शायद नहीं।
क्या जीवन एक केंद्र बिंदु है,
पता नहीं।
संभवतः जीवन का मूल,
ना तो लक्ष्य साधने में है न प्राप्त करने में,
ना अधिकार में है ना क्षति में,
ना विजय में है ना पराजय में।
कदाचित,
जीवन केवल एक यात्रा है।
जिसमें हमारा स्थूल शरीर एक यात्री है।
इस जीवन रूपी सफर में,
वह अनेक रंग के भोग भोगता है।
इसका अभाव-प्रभाव हमारे शरीर पर होता है जीवन पर नहीं।
तो फिर यह दुनिया भर के प्रपंच क्यों?
शायद,
जीवन की परिभाषा,
पूर्णता खोजने में है,
प्राप्त करने में नहीं।
शायद,
यही जीवन है।
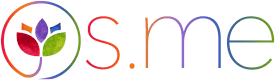








Comments & Discussion
2 COMMENTS
Please login to read members' comments and participate in the discussion.